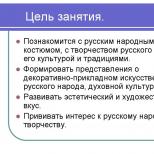साधारण ज्ञान: परिभाषा एवं अर्थ. संसार का ज्ञान. जीवनानुभव। दर्शनशास्त्र में अनुभूति
संज्ञान क्या है?
- कामुक,
- तर्कसंगत।
यह संज्ञान की सही परिभाषा है।
संज्ञानात्मक प्रक्रिया विभिन्न रूपों और सामग्रियों में ज्ञान का सामंजस्यपूर्ण विकास है। अर्थात्, अनुभूति को ज्ञान, सत्य और रचनात्मक गतिविधि की ओर मन की गति के रूप में समझा जाता है।
अनुभूति मनुष्य द्वारा विज्ञान के विभिन्न पहलुओं और प्रकृति की प्रकृति का अध्ययन है। नया ज्ञान प्राप्त करना. इस अवधारणा का दर्शनशास्त्र में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। हमारे आस-पास की दुनिया का ज्ञान या स्वयं का ज्ञान जैसी अवधारणाएँ हैं।
अनुभूति मनुष्य में अंतर्निहित है। अनुभूति नया ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है। अपने पूरे जीवन में एक व्यक्ति दुनिया का अनुभव करता है। एक छोटा नवजात बच्चा अपने चारों ओर देखता है, आवाज़ें सुनता है और इस तरह दुनिया के बारे में सीखता है। फिर हम जीवन भर लगातार कुछ न कुछ नया सीखते रहते हैं। सारा नया ज्ञान (जीवन के किसी भी क्षेत्र में) अनुभूति होगा।
अनुभूति- यह जानकारी, ज्ञान, अनुभव और वह सब कुछ है जो एक व्यक्ति विज्ञान से जानता है। और उस समय पर ही, अनुभूति- यह तब होता है जब ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया होती है, जब वस्तुनिष्ठ दुनिया के नियमों को समझा जाता है। और, निःसंदेह, प्रक्रिया के लिए ही ज्ञानकुछ योग्यताओं की आवश्यकता है. यह अकारण नहीं है कि यह कहता है:
अनुभूति किसी व्यक्ति द्वारा नया ज्ञान प्राप्त करने, पहले से अज्ञात किसी चीज़ की खोज करने की प्रक्रिया है। अनुभूति की प्रभावशीलता मुख्य रूप से इस प्रक्रिया में मनुष्य की सक्रिय भूमिका से प्राप्त होती है, जिसके लिए इसके दार्शनिक विचार की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में, हम पूर्वापेक्षाओं और परिस्थितियों, सत्य की ओर बढ़ने की शर्तों को स्पष्ट करने और इसके लिए आवश्यक तरीकों और अवधारणाओं में महारत हासिल करने के बारे में बात कर रहे हैं।
ज्ञान की दार्शनिक समस्याएं ज्ञान के सिद्धांत, या ज्ञानमीमांसा का विषय बनती हैं। ज्ञानमीमांसा ग्रीक मूल का शब्द है (ग्नोसिस ज्ञान और लोगो शब्द, शिक्षण)। ज्ञान का सिद्धांत इन प्रश्नों का उत्तर देता है कि ज्ञान क्या है, इसके मुख्य रूप क्या हैं, अज्ञान से ज्ञान में संक्रमण के पैटर्न क्या हैं, ज्ञान का विषय और वस्तु क्या है, संज्ञानात्मक प्रक्रिया की संरचना क्या है, सत्य क्या है और इसकी कसौटी क्या है, साथ ही और भी बहुत कुछ। ज्ञान के सिद्धांत शब्द को 1854 में स्कॉटिश दार्शनिक जे. फेरियर द्वारा दर्शनशास्त्र में पेश किया गया था।
ज्ञान के साधनों में सुधार करना मानव गतिविधि के इतिहास का एक अभिन्न अंग है। अतीत के कई दार्शनिकों ने ज्ञान के प्रश्नों के विकास की ओर रुख किया, और यह कोई संयोग नहीं है कि यह समस्या सामने आती है और दार्शनिक विचार के विकास में निर्णायक बन जाती है। सबसे पहले, ज्ञान अनुभवहीन, कभी-कभी बहुत ही आदिम रूपों में प्रकट होता है, अर्थात यह सामान्य ज्ञान के रूप में मौजूद होता है। इसके कार्य ने आज तक अपना महत्व नहीं खोया है। जैसे-जैसे मानव अभ्यास विकसित होता है, वास्तविक दुनिया को समझने में लोगों के कौशल और क्षमताओं में सुधार होता है, विज्ञान न केवल ज्ञान, बल्कि भौतिक उत्पादन का भी सबसे महत्वपूर्ण साधन बन जाता है। वैज्ञानिक ज्ञान के सिद्धांतों की पहचान की जाती है, जो वैज्ञानिक सोच के गठन और संगठन का आधार बने। साथ ही, सामान्य दार्शनिक सिद्धांतों की पहचान की जाती है जो संपूर्ण विश्व और अनुभूति के क्षेत्र (दुनिया के साथ मानव अनुभूति का संबंध), विशेष वैज्ञानिक सोच के सिद्धांत और विशेष वैज्ञानिक सिद्धांतों के सिद्धांतों पर लागू होते हैं।
विज्ञान 20वीं सदी में समाज के जीवन को बदलने वाले सबसे शक्तिशाली कारकों में से एक बन गया (सामाजिक चेतना के रूप में विज्ञान के बारे में अध्याय VIII में अधिक चर्चा की जाएगी)। इसने, बदले में, उसे सावधानीपूर्वक और गहन अध्ययन की वस्तु में बदल दिया। अनुसंधान का एक व्यापक मोर्चा विकसित हुआ, जिसका केंद्र मनुष्य और समाज की संज्ञानात्मक गतिविधि थी। वैज्ञानिक रचनात्मकता का मनोविज्ञान, विज्ञान का तर्क, विज्ञान का समाजशास्त्र, विज्ञान का इतिहास और अंत में, विज्ञान अध्ययन विशेष विषयों की एक छोटी सूची है जो ज्ञान की विभिन्न शाखाओं और रूपों का अध्ययन करते हैं। दर्शनशास्त्र भी अलग नहीं रहा, जिसने एक व्यापक क्षेत्र का निर्माण किया जिसे विज्ञान का दर्शन कहा जाता है (जिसमें कई उपखंड शामिल हैं: जीव विज्ञान का दर्शन, भौतिकी का दर्शन, गणित का दर्शन)।
अनुभूति मूल कारणों, उद्देश्यों, प्रकृति का ज्ञान है।
आपके अपने शब्दों में, ज्ञान किसी भी क्षेत्र में किसी नई चीज़ का अध्ययन है। मैं ज्ञान को गहन अध्ययन, अंदर से एक प्रकार का दृष्टिकोण कहूंगा। ज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ स्वयं जानने की इच्छा है। जब कोई व्यक्ति इच्छा के साथ किसी विषय का अध्ययन करता है, तो जानकारी बहुत बेहतर तरीके से अवशोषित होती है। हम बारीकियों, छोटी चीज़ों और अस्पष्ट मुद्दों की तलाश करते हैं और फिर उन्हें हल करते हैं। यह सब निश्चित रूप से एक निश्चित विषय में बेहतर ज्ञान प्रदान करता है। आप पढ़ा सकते हैं और अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण नहीं जानते।
अनुभूति व्यक्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस क्षमता के लिए धन्यवाद, हम विकसित होते हैं। अनुभूति एक प्रकार की मानवीय गतिविधि है जिसका उद्देश्य दुनिया के बारे में ज्ञान खोजना और प्राप्त करना है। अनुभूति के उद्देश्य यह समझने की इच्छा से निर्धारित होते हैं कि यह कैसे काम करता है और इसका उपयोग कैसे करें। अनुभूति का अंतिम लक्ष्य सत्य की प्राप्ति है
ज्ञान शब्द की परिभाषा इस प्रकार है:
यह वास्तविकता के प्रतिबिंब की उच्चतम डिग्री है, वास्तविक ज्ञान का विकास, जो एक व्यक्ति द्वारा जीवन के अनुभव के अधिग्रहण के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। यह एक व्यक्ति की कुछ नई चीज़ की इच्छा है, जो अभी तक समझ में नहीं आई है। ज्ञान के कई रूप हैं, लेकिन मुख्य है सत्य का ज्ञान।
यहां तार्किक शब्दकोश में शब्द की परिभाषा दी गई है:
यह ज्ञान में वृद्धि है. हमारी आभासी दुनिया का आकार बढ़ाना और उसकी गुणवत्ता बदलना। ज्ञान से ज्ञान उत्पन्न होता है। और ज्ञान ज्ञान को प्रोत्साहित करता है।
मैं ज्ञान शब्द को वास्तव में एक व्यक्ति की अपने लिए कुछ नया सीखने की प्रबल इच्छा के रूप में समझता हूं। इसे सटीक रूप से इच्छा में, स्वयं व्यक्ति की इच्छा में व्यक्त किया जाना चाहिए। किसी भी उद्योग में ज्ञान व्यक्ति को खुद को बेहतर बनाने और ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करता है। यह व्यक्ति को आगे बढ़ाता है, उसका विकास करता है।
अनुभूतिऐसी प्रक्रियाओं और विधियों के नाम बताइए जिनके द्वारा वस्तुगत जगत के नियमों और घटनाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ज्ञानमीमांसा का विज्ञान ज्ञान से संबंधित है।
जब हम अनुभूति के बारे में बात करते हैं, तो हमारा मतलब मानव रचनात्मक गतिविधि से होता है। इस प्रक्रिया में दो स्तर शामिल हैं:
यह यादृच्छिक और व्यवस्थित भी हो सकता है.
हर कोई इस शब्द में कुछ अलग देखता है... कुछ के लिए यह ज्ञान है... कुछ के लिए यह अनुभव और ज्ञान है, दूसरों के लिए यह आत्मज्ञान और भगवान है। यह सब व्यक्ति पर, उसके चरित्र पर और, तदनुसार, जीवन में उसकी स्थिति पर निर्भर करता है।
अनुभूति हमारे आसपास की दुनिया और अपने बारे में ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है। ज्ञान उस क्षण से शुरू होता है जब कोई व्यक्ति खुद से प्रश्न पूछना शुरू करता है: मैं कौन हूं, मैं इस दुनिया में क्यों आया, मुझे किस मिशन को पूरा करना चाहिए। अनुभूति एक सतत प्रक्रिया है. यह तब भी होता है जब किसी व्यक्ति को यह पता नहीं होता है कि कौन से विचार उसके कार्यों और कार्यों को निर्देशित करते हैं। एक प्रक्रिया के रूप में अनुभूति का अध्ययन कई विज्ञानों द्वारा किया जाता है: मनोविज्ञान, दर्शनशास्त्र, समाजशास्त्र, वैज्ञानिक पद्धति, इतिहास, विज्ञान। किसी भी ज्ञान का उद्देश्य स्वयं को बेहतर बनाना और अपने क्षितिज का विस्तार करना है।
अनुभूति की संरचना
एक वैज्ञानिक श्रेणी के रूप में अनुभूति की स्पष्ट रूप से परिभाषित संरचना होती है। अनुभूति में आवश्यक रूप से एक विषय और एक वस्तु शामिल होती है।विषय को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में समझा जाता है जो संज्ञान को क्रियान्वित करने के लिए सक्रिय कदम उठाता है। अनुभूति का उद्देश्य वह है जिस पर विषय का ध्यान निर्देशित किया जाता है। अनुभूति की वस्तु अन्य लोग, प्राकृतिक और सामाजिक घटनाएँ या कोई भी वस्तु हो सकती है।
अनुभूति के तरीके
अनुभूति के तरीकों को ऐसे उपकरण के रूप में समझा जाता है जिनकी मदद से हमारे आसपास की दुनिया के बारे में नया ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। अनुभूति के तरीकों को पारंपरिक रूप से अनुभवजन्य और सैद्धांतिक में विभाजित किया गया है।
अनुभूति के अनुभवजन्य तरीके
अनुभूति के अनुभवजन्य तरीकों में प्रयोगात्मक रूप से पुष्टि की गई किसी भी शोध गतिविधियों का उपयोग करके किसी वस्तु का अध्ययन शामिल है। अनुभूति के अनुभवजन्य तरीकों में शामिल हैं: अवलोकन, प्रयोग, माप, तुलना।
- अवलोकनअनुभूति की एक विधि है जिसके दौरान किसी वस्तु का उसके साथ सीधे संपर्क के बिना अध्ययन किया जाता है। दूसरे शब्दों में, पर्यवेक्षक ज्ञान की वस्तु से दूरी पर हो सकता है और फिर भी उसे आवश्यक जानकारी प्राप्त हो सकती है। अवलोकन की सहायता से, विषय किसी विशेष मुद्दे पर अपने निष्कर्ष निकाल सकता है और अतिरिक्त धारणाएँ बना सकता है। मनोवैज्ञानिकों, चिकित्सा कर्मियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा अपनी गतिविधियों में अवलोकन पद्धति का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
- प्रयोगअनुभूति की एक विधि है जिसमें विसर्जन एक विशेष रूप से निर्मित वातावरण में होता है। अनुभूति की इस पद्धति में बाहरी दुनिया से कुछ अमूर्तता शामिल है। प्रयोगों का उपयोग करके वैज्ञानिक अनुसंधान किया जाता है। अनुभूति की इस पद्धति के दौरान, आगे रखी गई परिकल्पना की पुष्टि या खंडन किया जाता है।
- मापअनुभूति की वस्तु के किसी भी पैरामीटर का विश्लेषण है: वजन, आकार, लंबाई, आदि। तुलना के दौरान ज्ञान की वस्तु की महत्वपूर्ण विशेषताओं की तुलना की जाती है।
अनुभूति के सैद्धांतिक तरीके
अनुभूति के सैद्धांतिक तरीकों में विभिन्न श्रेणियों और अवधारणाओं के विश्लेषण के माध्यम से किसी वस्तु का अध्ययन शामिल है। सामने रखी गई परिकल्पना की सत्यता की प्रयोगात्मक रूप से पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन मौजूदा अभिधारणाओं और अंतिम निष्कर्षों का उपयोग करके सिद्ध किया गया है। अनुभूति के सैद्धांतिक तरीकों में शामिल हैं: विश्लेषण, संश्लेषण, वर्गीकरण, सामान्यीकरण, संक्षिप्तीकरण, अमूर्तता, सादृश्य, कटौती, प्रेरण, आदर्शीकरण, मॉडलिंग, औपचारिकीकरण।
- विश्लेषणइसका तात्पर्य ज्ञान की संपूर्ण वस्तु का छोटे-छोटे भागों में मानसिक विश्लेषण करना है। विश्लेषण से घटकों, उनके अंतर और अन्य विशेषताओं के बीच संबंध का पता चलता है। अनुभूति की एक विधि के रूप में विश्लेषण का व्यापक रूप से वैज्ञानिक और अनुसंधान गतिविधियों में उपयोग किया जाता है।
- संश्लेषणइसमें अलग-अलग हिस्सों को एक पूरे में जोड़ना, उनके बीच एक कनेक्टिंग लिंक की खोज करना शामिल है। सभी अनुभूति की प्रक्रिया में संश्लेषण का सक्रिय रूप से उपयोग किया जाता है: नई जानकारी को स्वीकार करने के लिए, इसे मौजूदा ज्ञान के साथ सहसंबंधित करना आवश्यक है।
- वर्गीकरणविशिष्ट मापदंडों के अनुसार एकजुट वस्तुओं का एक समूह है।
- सामान्यकरणइसमें अलग-अलग वस्तुओं को उनकी मुख्य विशेषताओं के अनुसार समूहीकृत करना शामिल है।
- विनिर्देशकिसी वस्तु या घटना के महत्वपूर्ण विवरणों पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से की जाने वाली एक स्पष्टीकरण प्रक्रिया है।
- मतिहीनताइसका तात्पर्य एक नए दृष्टिकोण की खोज करने के लिए, अध्ययन की जा रही समस्या पर एक अलग दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए किसी विशेष विषय के विशेष पक्ष पर ध्यान केंद्रित करना है। साथ ही, अन्य घटकों पर विचार नहीं किया जाता है, उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है, या उन पर अपर्याप्त ध्यान दिया जाता है।
- समानताअनुभूति की वस्तु में समान वस्तुओं की उपस्थिति की पहचान करने के लिए किया गया।
- कटौती- यह अनुभूति की प्रक्रिया में सिद्ध निष्कर्षों के परिणामस्वरूप सामान्य से विशिष्ट की ओर संक्रमण है।
- प्रेरण- यह अनुभूति की प्रक्रिया में सिद्ध निष्कर्षों के परिणामस्वरूप विशेष से संपूर्ण की ओर एक संक्रमण है।
- आदर्श बनानाइसका तात्पर्य किसी ऐसी वस्तु को दर्शाने वाली अलग-अलग अवधारणाओं का निर्माण है जो वास्तविकता में मौजूद नहीं है।
- मोडलिंगअनुभूति की प्रक्रिया में मौजूदा वस्तुओं की किसी भी श्रेणी का निर्माण और लगातार अध्ययन शामिल है।
- औपचारिकआम तौर पर स्वीकृत प्रतीकों का उपयोग करके वस्तुओं या घटनाओं को प्रतिबिंबित करता है: अक्षर, संख्याएं, सूत्र या अन्य प्रतीक।
ज्ञान के प्रकार
अनुभूति के प्रकारों को मानव चेतना की मुख्य दिशाओं के रूप में समझा जाता है, जिनकी सहायता से अनुभूति की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। कभी-कभी उन्हें अनुभूति के रूप भी कहा जाता है।
साधारण अनुभूति
इस प्रकार की अनुभूति का तात्पर्य है कि एक व्यक्ति जीवन गतिविधि की प्रक्रिया में अपने आसपास की दुनिया के बारे में बुनियादी जानकारी प्राप्त करता है। एक बच्चे में भी सामान्य ज्ञान होता है। एक छोटा व्यक्ति, आवश्यक ज्ञान प्राप्त करके, अपने निष्कर्ष निकालता है और अनुभव प्राप्त करता है। यदि कोई नकारात्मक अनुभव भी आता है, तो भविष्य में यह सावधानी, सावधानी और विवेक जैसे गुणों को विकसित करने में मदद करेगा। प्राप्त अनुभव को समझने और उसे आंतरिक रूप से जीने से एक जिम्मेदार दृष्टिकोण विकसित होता है। रोजमर्रा के ज्ञान के परिणामस्वरूप, एक व्यक्ति को यह विचार विकसित होता है कि वह जीवन में कैसे कार्य कर सकता है और क्या नहीं, उसे किस पर भरोसा करना चाहिए और किस बारे में भूलना चाहिए। साधारण अनुभूति दुनिया के बारे में प्राथमिक विचारों और मौजूदा वस्तुओं के बीच संबंधों पर आधारित है। यह सामान्य सांस्कृतिक मूल्यों को प्रभावित नहीं करता है, व्यक्ति के विश्वदृष्टिकोण, उसके धार्मिक और नैतिक अभिविन्यास पर विचार नहीं करता है। साधारण अनुभूति केवल आसपास की वास्तविकता के बारे में क्षणिक अनुरोध को संतुष्ट करने का प्रयास करती है। एक व्यक्ति बस आगे की जीवन गतिविधियों के लिए आवश्यक उपयोगी अनुभव और ज्ञान जमा करता है।
वैज्ञानिक ज्ञान
इस प्रकार की अनुभूति तार्किक दृष्टिकोण पर आधारित होती है।इसका दूसरा नाम है. यहां उस स्थिति का विस्तृत विचार जिसमें विषय डूबा हुआ है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए, मौजूदा वस्तुओं का विश्लेषण किया जाता है और उचित निष्कर्ष निकाले जाते हैं। किसी भी दिशा की अनुसंधान परियोजनाओं में वैज्ञानिक ज्ञान का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। विज्ञान की सहायता से अनेक तथ्य सत्य अथवा असिद्ध सिद्ध किये जाते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण कई घटकों के अधीन है; कारण और प्रभाव संबंध एक बड़ी भूमिका निभाते हैं।
वैज्ञानिक गतिविधि में, अनुभूति की प्रक्रिया परिकल्पनाओं को सामने रखकर और उन्हें व्यवहार में सिद्ध करके की जाती है। शोध के परिणामस्वरूप, वैज्ञानिक अपनी धारणाओं की पुष्टि कर सकता है या उन्हें पूरी तरह से त्याग सकता है यदि अंतिम उत्पाद बताए गए लक्ष्य को पूरा नहीं करता है। वैज्ञानिक ज्ञान मुख्यतः तर्क और सामान्य ज्ञान पर आधारित होता है।
कलात्मक ज्ञान
इस प्रकार के संज्ञान को रचनात्मक भी कहा जाता है। ऐसा ज्ञान कलात्मक छवियों पर आधारित होता है और व्यक्ति की गतिविधि के बौद्धिक क्षेत्र को प्रभावित करता है। यहां किसी भी कथन की सत्यता को वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि कलाकार सौंदर्य की श्रेणी के संपर्क में आता है। वास्तविकता कलात्मक छवियों में प्रतिबिंबित होती है, और मानसिक विश्लेषण की विधि द्वारा निर्मित नहीं होती है। कलात्मक ज्ञान अपने सार में असीमित है। दुनिया के रचनात्मक ज्ञान की प्रकृति ऐसी है कि व्यक्ति स्वयं विचारों और विचारों की मदद से अपने सिर में एक छवि बनाता है। इस तरह से बनाई गई सामग्री एक व्यक्तिगत रचनात्मक उत्पाद है और अस्तित्व का अधिकार प्राप्त करती है। प्रत्येक कलाकार की अपनी आंतरिक दुनिया होती है, जिसे वह रचनात्मक गतिविधि के माध्यम से अन्य लोगों के सामने प्रकट करता है: एक कलाकार चित्र बनाता है, एक लेखक किताबें लिखता है, एक संगीतकार संगीत बनाता है। हर रचनात्मक सोच का अपना सच और कल्पना होती है।
दार्शनिक ज्ञान
इस प्रकार की अनुभूति में दुनिया में किसी व्यक्ति का स्थान निर्धारित करके वास्तविकता की व्याख्या करने का इरादा शामिल होता है। दार्शनिक ज्ञान की विशेषता व्यक्तिगत सत्य की खोज, जीवन के अर्थ पर निरंतर प्रतिबिंब, विवेक, विचारों की शुद्धता, प्रेम, प्रतिभा जैसी अवधारणाओं के लिए अपील है। दर्शन सबसे जटिल श्रेणियों के सार में प्रवेश करने, रहस्यमय और शाश्वत चीजों की व्याख्या करने, मानव अस्तित्व का सार निर्धारित करने और पसंद के अस्तित्व संबंधी प्रश्नों को निर्धारित करने का प्रयास करता है। दार्शनिक ज्ञान का उद्देश्य अस्तित्व के विवादास्पद मुद्दों को समझना है। अक्सर, ऐसे शोध के परिणामस्वरूप, कार्यकर्ता को सभी चीजों की दुविधा समझ में आती है। दार्शनिक दृष्टिकोण में किसी वस्तु, घटना या निर्णय के दूसरे (छिपे हुए) पक्ष को देखना शामिल है।
धार्मिक ज्ञान
इस प्रकार की अनुभूति का उद्देश्य उच्च शक्तियों के साथ मानवीय संबंधों का अध्ययन करना है।यहां सर्वशक्तिमान को एक साथ अध्ययन की वस्तु और एक विषय के रूप में माना जाता है, क्योंकि धार्मिक चेतना का तात्पर्य ईश्वरीय सिद्धांत की प्रशंसा से है। एक धार्मिक व्यक्ति सभी वर्तमान घटनाओं की व्याख्या ईश्वरीय विधान के दृष्टिकोण से करता है। वह अपनी आंतरिक स्थिति, मनोदशा का विश्लेषण करता है और जीवन में किए गए कुछ कार्यों के लिए ऊपर से कुछ विशिष्ट प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करता है। उनके लिए किसी भी व्यवसाय का आध्यात्मिक घटक, नैतिकता और नैतिक सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण हैं। ऐसा व्यक्ति अक्सर ईमानदारी से दूसरों की खुशी की कामना करता है और सर्वशक्तिमान की इच्छा को पूरा करना चाहता है। धार्मिक विचारधारा वाली चेतना का तात्पर्य एकमात्र सही सत्य की खोज है, जो कई लोगों के लिए उपयोगी होगा, न कि किसी विशिष्ट व्यक्ति के लिए। प्रश्न जो व्यक्ति से पूछे जाते हैं: अच्छाई और बुराई क्या है, विवेक के अनुसार कैसे जीना है, हम में से प्रत्येक का पवित्र कर्तव्य क्या है।
पौराणिक ज्ञान
इस प्रकार की अनुभूति आदिम समाज की है. यह उस व्यक्ति के ज्ञान का संस्करण है जो स्वयं को प्रकृति का अभिन्न अंग मानता था। प्राचीन लोगों ने आधुनिक लोगों की तुलना में जीवन के सार के बारे में सवालों के जवाब अलग तरह से खोजे; उन्होंने प्रकृति को दैवीय शक्ति से संपन्न किया। यही कारण है कि पौराणिक चेतना ने अपने देवताओं और वर्तमान घटनाओं के प्रति तदनुरूप दृष्टिकोण का गठन किया। आदिम समाज ने रोजमर्रा की वास्तविकता में जो कुछ भी घटित हुआ उसकी जिम्मेदारी छोड़ दी और पूरी तरह से प्रकृति की ओर मुड़ गया।
आत्मज्ञान
इस प्रकार के संज्ञान का उद्देश्य किसी की वास्तविक स्थिति, मनोदशा और निष्कर्ष का अध्ययन करना है। आत्म-ज्ञान में हमेशा किसी की अपनी भावनाओं, विचारों, कार्यों, आदर्शों और आकांक्षाओं का गहन विश्लेषण शामिल होता है। जो लोग कई वर्षों से सक्रिय रूप से आत्म-ज्ञान में लगे हुए हैं, उन्होंने ध्यान दिया कि उनके पास अत्यधिक विकसित अंतर्ज्ञान है। ऐसा व्यक्ति भीड़ में नहीं खोएगा, "झुंड" की भावना के आगे नहीं झुकेगा, बल्कि स्वयं जिम्मेदार निर्णय लेगा। आत्म-ज्ञान एक व्यक्ति को उसके उद्देश्यों को समझने, उसके द्वारा जीए गए वर्षों और उसके द्वारा किए गए कार्यों को समझने में मदद करता है। आत्म-ज्ञान के परिणामस्वरूप, व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक गतिविधि बढ़ती है, वह आत्मविश्वास जमा करता है, और वास्तव में साहसी और उद्यमी बन जाता है।
इस प्रकार, आसपास की वास्तविकता के बारे में आवश्यक ज्ञान प्राप्त करने की एक गहरी प्रक्रिया के रूप में अनुभूति की अपनी संरचना, तरीके और प्रकार होते हैं। प्रत्येक प्रकार का ज्ञान सामाजिक विचार के इतिहास में एक अलग अवधि और किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत पसंद से मेल खाता है।
विषय की रचनात्मक गतिविधि, दुनिया के बारे में विश्वसनीय ज्ञान प्राप्त करने पर केंद्रित है। पी. संस्कृति के अस्तित्व की एक अनिवार्य विशेषता है और, इसके कार्यात्मक उद्देश्य, ज्ञान की प्रकृति और संबंधित साधनों और विधियों के आधार पर, निम्नलिखित रूपों में किया जा सकता है: रोजमर्रा, पौराणिक, धार्मिक, कलात्मक, दार्शनिक और वैज्ञानिक .
पी की प्रारंभिक संरचना को विषय-वस्तु संबंध द्वारा दर्शाया गया है, जहां किसी वस्तु की आवश्यक विशेषताओं (सच्चाई की समस्या) के विषय द्वारा पर्याप्त पुनरुत्पादन की संभावना का प्रश्न ज्ञानमीमांसा (सिद्धांत) का केंद्रीय विषय है पी. का) इस मुद्दे के समाधान के आधार पर, दर्शन संज्ञानात्मक आशावाद, संदेहवाद और अज्ञेयवाद की स्थिति को अलग करता है। सत्य पी के सार्वभौमिक लक्ष्य के रूप में कार्य करता है। साथ ही, ऐतिहासिक और दार्शनिक परंपरा के संदर्भ में सत्य और इसे प्राप्त करने के तरीकों के बारे में विचारों को "ज्ञान और राय" (प्राचीनता) के मौलिक विरोधों को अलग करके ठोस बनाया गया था। "कारण और विश्वास" (मध्य युग), "ज्ञान और अज्ञान" (नया समय)। विषय-वस्तु संबंधों की प्रकृति को समझना पी की प्रकृति पर संबंधित विचारों को निर्धारित करता है। शास्त्रीय दर्शन के लिए, पी की प्रक्रिया चिंतन है, जो वस्तुनिष्ठ वास्तविकता के पूर्ण और अपरिवर्तनीय कानूनों की धारणा में विषय की निष्क्रिय भूमिका को मानती है। जो उसके लिए बाहरी हैं. इस मामले में, पी. की व्याख्या दो मुख्य दृष्टिकोणों से की जा सकती है: 1) पी. की व्याख्या, स्मरण के रूप में, प्लेटो पर वापस जाकर और मुख्य रूप से तर्कसंगत-आदर्शवादी परंपरा (इनामनेसिस के सिद्धांत) के संदर्भ में विकसित हुई; 2) प्रतिबिंब के रूप में पी. की विशेषता, भौतिकवाद और अनुभववाद के मॉडल में सबसे स्पष्ट रूप से महसूस की गई।
आई. कांट के "कोपरनिकन मोड़" से शुरू होकर, दर्शन ज्ञानमीमांसा में चिंतनशील वस्तुवाद से दूर चला जाता है और संज्ञानात्मक प्रक्रिया में विषय की सक्रिय भूमिका को साकार करता है। जर्मन आदर्शवाद के लिए, पी. में खुलने वाली दुनिया पहले से ही एक पारलौकिक विषय (कांट, आई.जी. फिचटे, एफ. शेलिंग) की रचनात्मकता का प्रक्षेपण या एक सामाजिक-ऐतिहासिक विषय (जी. हेगेल) की गतिविधि का उत्पाद है। एक रचनात्मक गतिविधि के रूप में कविता की व्याख्या आधुनिक गैर-शास्त्रीय दर्शन को अलग करती है। यह विशेषता है कि, संज्ञानात्मक प्रक्रिया में विषय की रचनात्मक स्थिति पर जोर देते हुए, आधुनिक दर्शन ने बड़े पैमाने पर न केवल शास्त्रीय विचार के ऑन्कोलॉजी को त्याग दिया है, बल्कि उद्देश्य सत्य की स्थापना भी की है, जो वास्तव में सामाजिक-ऐतिहासिक, व्यावहारिक और विषय के मनोवैज्ञानिक हित. यहां संज्ञानात्मक गतिविधि की प्रकृति को प्रैक्सियोलॉजिकल, सिमेंटिक और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के संदर्भ में माना जा सकता है। आधुनिक दर्शन में दर्शन की व्यावहारिक प्रकृति पर जोर मुख्य रूप से मार्क्सवाद और व्यावहारिकता की विशेषता है। हालाँकि, यदि मार्क्सवाद में पी., वास्तविकता के उन्नत प्रतिबिंब का एक रूप होने के नाते, समाज के प्रकृति-परिवर्तनकारी और सामाजिक-ऐतिहासिक अभ्यास में सबसे महत्वपूर्ण क्षण के रूप में कार्य करता है, तो व्यावहारिकता में पी., संदेह पर काबू पाते हुए, विषय को मनोवैज्ञानिक प्रदान करता है उसकी क्षमताओं पर विश्वास, जिससे उसे व्यावहारिक गतिविधि को सबसे प्रभावी ढंग से करने की अनुमति मिलती है। पी. के लिए अर्थ संबंधी दृष्टिकोण आज घटना विज्ञान और हेर्मेनेयुटिक्स के ढांचे के भीतर लागू किया गया है। पी. यहां अर्थ निर्माण की एक प्रक्रिया है, जो किसी व्यक्ति को बाहरी वास्तविकता की नहीं बल्कि स्वयं की समझ के क्षितिज का विस्तार करने की अनुमति देती है। और, अंत में, विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण नव- और उत्तर-सकारात्मकता और संरचनावाद की धाराओं से जुड़ा हुआ है, जो मनोविज्ञान को संकेत संरचनाओं के वैज्ञानिक विश्लेषण के रूप में मानने की ओर उन्मुख है जो कमोबेश मौजूदा तार्किक और लाक्षणिक अपरिवर्तनीयता का पर्याप्त रूप से वर्णन करता है, लेकिन किसी भी तरह से दावा नहीं करता है। उनकी सच्ची समझ बनें।
संज्ञानात्मक प्रक्रिया की संरचना में, पी. के संवेदी और तर्कसंगत स्तर भी प्रतिष्ठित हैं, जिसके आधुनिक यूरोपीय दर्शन में विरोध के कारण तर्कवाद और अनुभववाद की दुविधा का उदय हुआ। संवेदी धारणा (इसके मुख्य रूप: संवेदना, धारणा और प्रतिनिधित्व) विषय और वस्तु के बीच सीधे संपर्क का परिणाम है, जो यहां प्राप्त ज्ञान की विशिष्टता, व्यक्तित्व और स्थितिजन्य प्रकृति को निर्धारित करता है। सामान्य रूप से संज्ञानात्मक गतिविधि का आधार होने के नाते, पी. का संवेदी स्तर कला और रोजमर्रा के अभ्यास में विशेष महत्व रखता है। तर्कसंगत दर्शन (इसके रूप: अवधारणा, निर्णय और अनुमान) व्यक्तिगत ज्ञान को वस्तुनिष्ठ बनाने, उसके सामान्यीकरण, अनुवाद आदि की संभावना मानता है। यह तर्कसंगत दर्शन है जो विज्ञान और दर्शन जैसे संज्ञानात्मक रचनात्मकता के ऐसे रूपों के अस्तित्व को सुनिश्चित करता है। संवेदी और तर्कसंगत के अलावा, अंतर्ज्ञान संज्ञानात्मक प्रक्रिया में एक विशेष भूमिका निभाता है, जो मानस की अचेतन संरचनाओं के स्तर पर धारणा के विशेष तंत्र का संकेत देता है। पी. को पी. की वस्तु और उसके अनुरूप ज्ञान के प्रकार के आधार पर भी संरचित किया जा सकता है। शिक्षाशास्त्र की सबसे सामान्य वस्तुओं में प्रकृति, समाज और मनुष्य और उनसे जुड़ा प्राकृतिक, सामाजिक और मानवीय ज्ञान शामिल है। एक विशेष प्रकार का दर्शन आत्म-ज्ञान है, जो सुकरात के समय से, दर्शन में केंद्रीय विषयों में से एक रहा है और साथ ही व्यक्तिगत अस्तित्व के सबसे महत्वपूर्ण तरीकों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। मनोविज्ञान की समस्याओं का अध्ययन आज कई दार्शनिक (ज्ञानमीमांसा, ज्ञानमीमांसा, सांस्कृतिक अध्ययन, तर्कशास्त्र और विज्ञान की पद्धति) और विशेष (संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, वैज्ञानिक अध्ययन, ज्ञान और विज्ञान का समाजशास्त्र, आदि) विषयों द्वारा किया जाता है।
अपने अस्तित्व और विकास के लंबे सफर के दौरान, मनुष्य का झुकाव अनुसंधान, अध्ययन और खोजों की ओर था। उन्होंने अपने जीवन को सरल बनाने के लिए बहुत कुछ किया, अपने अस्तित्व के अर्थ, प्राकृतिक घटनाओं के किसी भी पैटर्न और कारणों की खोज के लिए बहुत प्रयास किए।
घटना का सार
ज्ञान की अवधारणा की व्याख्या काफी व्यापक रूप से की गई है। सबसे सामान्य अर्थ में, इसे एक प्रक्रिया या तंत्र के एक पूरे सेट के रूप में समझा जाता है जो हमें दुनिया का अध्ययन करने, इसके बारे में वस्तुनिष्ठ डेटा जमा करने और विभिन्न प्रकार के पैटर्न की पहचान करने में मदद करता है। इस घटना की भूमिका को कम करके आंकना कठिन है। क्योंकि यह उन्हीं की बदौलत था कि लोगों ने तकनीकी, चिकित्सा, तकनीकी और अन्य सफलताएँ हासिल कीं जिन्हें हम अब देख सकते हैं। सामाजिक विज्ञान हमें इस अवधारणा के बारे में काफी व्यापक रूप से बताता है। रूप, इसके कार्य - यह सब हम स्कूल में सीख सकते हैं। हालाँकि, वह विज्ञान जो विशेष रूप से इस पहलू के अध्ययन के लिए समर्पित है, ज्ञानमीमांसा कहलाता है। और वह अंदर आती है
यह क्या है?
अनुभूति की प्रक्रिया बहुत जटिल और बहुआयामी है। इसका वर्णन करना, या इसे सरल रूपों में रखना काफी समस्याग्रस्त है। इसका तात्पर्य यह है कि हमें पहले अपने जीवन के इस पहलू की जटिल संरचना को समझना चाहिए, और फिर पूरी सभ्यता के लिए इसका उद्देश्य और महत्व निर्धारित करना चाहिए। व्यापक अर्थ में, अनुभूति की अवधारणा कमजोर रूप से प्रक्रिया के संपूर्ण सार को दर्शाती है। इसलिए, इसकी संरचना को स्पष्ट रूप से उजागर करना आवश्यक है।

यह किस तरह का है?
पहले, परिभाषा देते समय, हमने कहा था कि अनुभूति एक बहुआयामी तंत्र है। यह एक अकेली प्रक्रिया नहीं है, बल्कि अन्य महत्वपूर्ण तत्वों के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई एक पूरी प्रणाली है। दार्शनिक शब्दावली और विज्ञान में बहुत गहराई तक न जाने के लिए, हम उस पाठ्यक्रम और सिफारिशों पर निर्माण करेंगे जो विषय हमें देता है - सामाजिक विज्ञान। अनुभूति के प्रकार और अनुभूति के रूपों का अक्सर उपयोग किया जाता है, जिसका एक ही अर्थ होता है - तकनीकों और तरीकों का एक सेट जिसके माध्यम से अध्ययन के तहत प्रक्रिया होती है। आइए उनमें से प्रत्येक के बारे में अधिक विस्तार से बात करें।
परिवार
कई वैज्ञानिक अनुभूति के इस रूप को एक अलग श्रेणी में नहीं रखते हैं। हालाँकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि रोजमर्रा, रोजमर्रा के स्तर के बिना जीवन का ज्ञान लगभग असंभव है। इस प्रजाति को गंभीर अध्ययन की आवश्यकता नहीं है। इसका बारीकी से अध्ययन करने या विशेष उपकरणों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए, यह समझने के लिए कि आग का तापमान अधिक है, जल जाना ही काफी है। आपके पास मापने का कोई उपकरण नहीं होगा, लेकिन आप निश्चित रूप से कह पाएंगे: लौ बहुत गर्म है।
इस प्रकार, अनुभूति की रोजमर्रा की प्रक्रिया बेहद गलत है। वह हमारे प्रश्नों का केवल अनुमानित उत्तर ही देता है। हालाँकि, यह काफी जल्दी समझ में आ जाता है। यह तंत्र सहज है और इसे विकसित करने के लिए बहुत अधिक समय की आवश्यकता नहीं होती है। अनुभूति के इस रूप का सामना हम अपने दैनिक जीवन में सबसे अधिक बार करते हैं। एक नियम के रूप में, हम जितने बड़े होते हैं, इस प्रकार से हम उतना ही अधिक ज्ञान अर्जित करते हैं। लेकिन इतिहास कई अपवादों को जानता है।

वैज्ञानिक सामाजिक अनुभूति
इसे वैज्ञानिक विधि भी कहा जाता है। यह अनुभूति का सबसे सटीक, लेकिन श्रमसाध्य तरीका भी है। इसके लिए आपको कलात्मक गुण दिखाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि केवल सटीकता और अध्ययन के प्रति प्रेम की आवश्यकता है। इस पद्धति का उपयोग सामाजिक अध्ययन सहित सभी शैक्षणिक विषयों द्वारा किया जाता है। सामान्य तौर पर अनुभूति के प्रकार, किसी न किसी रूप में, इसी प्रकार पर आधारित होते हैं। आख़िरकार, इसकी सहायता से आप सरल ज्ञान को समझ सकते हैं, जो इसे और अधिक उपयोगी बना देगा।
यह रूप भी काफी विविध है. उदाहरण के लिए, एक वैज्ञानिक है। इसका उद्देश्य समाज, लोगों के संघों, सामाजिक समूहों और बहुत कुछ का अध्ययन करना है। सभी वैज्ञानिक विधियों को दो प्रकारों में विभाजित किया गया है - सैद्धांतिक और अनुभवजन्य। पहला धारणाएँ बनाता है, वास्तविक ज्ञान के अनुपालन के लिए उनकी जाँच करता है, मॉडल और संपूर्ण सिस्टम बनाता है। व्यावहारिक विधि प्रयोग, अवलोकन के माध्यम से परिकल्पनाओं की वास्तविकता का परीक्षण करती है और काल्पनिक विचारों में समायोजन भी करती है।
अनुभवजन्य ज्ञान नई घटनाओं को भी प्रकट कर सकता है जो तब सिद्धांतकारों द्वारा करीबी ध्यान का विषय होगा। हालाँकि ज्ञान के इस रूप को सबसे बड़ी संख्या में अनुयायी मिले हैं, लेकिन इसके बिना ऐसा नहीं किया जा सकता है, जो, मुझे कहना होगा, काफी उपयुक्त है। इस प्रकार, कुछ वैज्ञानिक बताते हैं कि नया ज्ञान विसंगतियाँ है। विज्ञान, अपनी राय में, कुछ अप्राकृतिक घटनाओं की खोज करके, विश्वदृष्टि की वास्तविक प्रणाली में अपने अस्तित्व को साबित करना शुरू कर देता है। इसके पैटर्न की पहचान करने की कोशिश करता है, साथ ही यह भी कि यह मौजूदा सिद्धांतों के ढांचे में फिट क्यों नहीं बैठता है।
अक्सर ऐसी विसंगतियाँ पूरी तरह से स्थापित राय का खंडन करती हैं। क्रांतिकारी परिकल्पनाओं को सिद्ध करने की कोशिश कर रहे कोपरनिकस या अन्य वैज्ञानिकों को याद रखें। उन्होंने ऐसी विसंगतियों की खोज की और उन्हें समझने का प्रयास किया, जिसके परिणामस्वरूप पहले से संचित ज्ञान उन्हें ग़लत लगने लगा। इस प्रकार, पहले लोग यह नहीं मानते थे कि पृथ्वी गोलाकार है या सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। इतिहास ऐसे कई उदाहरण जानता है - आइंस्टीन, गैलीलियो, मैगलन, आदि।

कलात्मक
कुछ लोग यह तर्क दे सकते हैं कि इस प्रकार में सामाजिक और मानवीय ज्ञान शामिल है। लेकिन यह सच नहीं है. यह रूप सबसे आकर्षक है. यह सबसे सरल और साथ ही सबसे जटिल भी है। मान लीजिए कि कई हजार साल पहले लोगों ने लेखन का अध्ययन करना शुरू किया था, और इससे पहले वे जानकारी देने के लिए केवल चित्रों का उपयोग करते थे। उन्होंने इसकी दृश्य छवि को एक माध्यम (उदाहरण के लिए, एक पत्थर) में स्थानांतरित करके प्राकृतिक घटनाओं का वर्णन किया। इसने अनुभव को स्थानांतरित करने के लिए पीढ़ियों के बीच बातचीत को बहुत सरल बना दिया।
इसके बाद, लोगों ने अधिक सुलभ संचार और सूचनाओं के आदान-प्रदान को सुनिश्चित करने के लिए भाषाओं का विकास और आविष्कार करना शुरू किया। प्रतीक, चित्र, छवियां - यह सब प्रारंभिक चरण में ही काफी सरल दिखता है। अब कलाकृति को देखो. उस अर्थ को समझने के लिए जो लेखक हमें बताना चाहते हैं, कुछ जानने के लिए, हमने जो देखा या पढ़ा है उसे समझने के लिए, लेखक द्वारा अपने विचारों को व्यक्त करने के तरीकों को समझने के लिए प्रयास करना आवश्यक है।
यह कहा जाना चाहिए कि यह रूप हमें कई जानवरों से महत्वपूर्ण रूप से अलग करता है, बल्कि एक-दूसरे से भी अधिक महत्वपूर्ण रूप से अलग करता है। आजकल, लोगों को आसानी से उन लोगों में विभाजित किया जा सकता है जो चीजों को चित्रित करने की कोशिश करते हैं, उन्हें अपनी आंतरिक दुनिया के चश्मे से गुजरते हैं, और जो सब कुछ वैसा ही देखते हैं जैसा वह है। यही कारण है कि कला का रूप अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण, उपयोगी और जटिल है, लेकिन यह कभी भी वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकता। इस प्रकार के संज्ञान की यही मुख्य समस्या है। आख़िरकार, यह व्यक्तिपरक दृष्टि के बजाय वस्तुनिष्ठ ज्ञान को पहचानने और संचय करने के लक्ष्य का अनुसरण करता है। फिर भी, इस फॉर्म का प्रयोग अक्सर किया जाता है। उन्होंने हमारी सभ्यता के विकास में भी बहुत बड़ा योगदान दिया।

दार्शनिक
दार्शनिक ज्ञान कई सदियों पहले मौजूद दुनिया और आपके और मेरे दोनों के लिए अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान है। केवल दार्शनिक ज्ञान के माध्यम से ही कोई वास्तविकता और अस्तित्व से परे जा सकता है। यह दार्शनिक ही थे जिन्होंने हमारी दुनिया और यहां तक कि ब्रह्मांड की संरचना के बारे में परिकल्पनाएं प्रस्तुत करना शुरू किया। इन सभी पहलुओं के अध्ययन के तरीकों के आविष्कार से पहले भी उन्होंने हमारे शरीर, हमारी सोच, सभी लोगों की विशेषताओं के बारे में बात की थी।
दार्शनिक ज्ञान को आमतौर पर दो प्रकारों में विभाजित किया जाता है - ज्ञानमीमांसा (या सामान्य) और सत्तामीमांसीय। दूसरा प्रकार सभी पक्षों से सार और अस्तित्व के अध्ययन पर आधारित है - वास्तविक, मानसिक, व्यक्तिपरक, वस्तुनिष्ठ, आदि। उल्लेखनीय बात यह है कि इस प्रकार के ज्ञान के माध्यम से लोगों ने न केवल अपने आस-पास की दुनिया को निर्धारित किया, बल्कि उसमें अपना स्थान भी पाया। इसने, लेकिन यह भी दिखाया कि यह जगह कैसी होनी चाहिए।
दर्शन अक्सर आदर्शीकरण के लिए प्रयास करता है, इसलिए इस प्रकार का ज्ञान प्रश्नों का उत्तर देता है: "यह कैसा है, यह कैसा होना चाहिए?" फिर से, काफी सामान्य शब्दों में। ऐसे सामान्य रूप हमें सामाजिक विज्ञान द्वारा दिए जाते हैं, जिनमें ज्ञान के प्रकार इतने पूर्ण रूप से प्रकट नहीं होते हैं कि दर्शन की सीमाओं का उल्लंघन न करें।

कदम
प्रकारों के अलावा, अनुभूति के स्तर भी प्रतिष्ठित हैं। कभी-कभी उन्हें रूपों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। लेकिन उनके बारे में उन चरणों के रूप में बात करना अधिक सही है जो सभी प्रकार में उपयोग किए जाते हैं। ऐसे केवल दो स्तर हैं। लेकिन वे हमारे जीवन में अविश्वसनीय रूप से बड़ी भूमिका निभाते हैं।
कामुक स्तर
यह हमारी इंद्रियों पर निर्मित होता है और पूरी तरह से उन पर निर्भर करता है। प्राचीन काल से, जब आधुनिक मनुष्य के वंशजों ने औजारों में महारत हासिल करना शुरू नहीं किया था, तब भी वे पहले से ही भावनाओं से संपन्न थे। रोजमर्रा के संज्ञान के प्रकार के बारे में सोचें। उदाहरण के लिए, अगर हम इसे महसूस नहीं कर पाते तो हम यह नहीं समझ पाएंगे कि आग गर्म है। हालाँकि बहुत से लोग 6 इंद्रियों के बारे में बात करते हैं, वास्तव में और भी हैं। इस प्रकार, सातवीं इंद्रिय को आकर्षण की भावना, तथाकथित गुरुत्वाकर्षण बल कहा जा सकता है।
संवेदी स्तर के रूप
सामान्य तौर पर, उनमें से केवल 3 हैं। वे कई इंद्रियों को जोड़ते हैं। ये निम्नलिखित तंत्र हैं:
- अनुभूति। किसी वस्तु के कुछ गुण हमें बताने में सक्षम। प्रत्येक इंद्रिय की विशिष्टता के कारण, हमें किसी विशेष चीज़, घटना या प्रक्रिया की विशेषताओं के बारे में एक "रिपोर्ट" प्राप्त होती है। सेब के उदाहरण का उपयोग करके हम कह सकते हैं कि दृष्टि की सहायता से हम रंग देखते हैं, स्पर्श की सहायता से हम उसकी कोमलता, तापमान, आकार, स्वाद कलिकाओं की सहायता से - स्वाद निर्धारित कर सकते हैं।
- धारणा। यह अधिक वैश्विक रूप है. इसके माध्यम से हमें सबसे संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, हम संवेदना के माध्यम से प्राप्त की गई हर चीज़ को एक समग्र चित्र में जोड़ते हैं। पहले पैराग्राफ में बताई गई सभी बातों को जोड़कर हम एक सेब की कई महत्वपूर्ण विशेषताओं को समझेंगे।
- प्रदर्शन। हमारी स्मृति के आधार पर. आपको किसी वस्तु की कामुक छवि बनाने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए, एक नींबू के बारे में सोचें, कैसे इसे सावधानी से टुकड़ों में काटा जाता है और नमक छिड़का जाता है। आप तुरंत अपने मुंह में लार की मात्रा बढ़ने के साथ-साथ खट्टा स्वाद भी महसूस करेंगे। नींबू का आकार, उसका रंग और अन्य विशेषताएं दिमाग में आ जाएंगी। प्रतिनिधित्व हमें जीवन में प्राप्त महत्वपूर्ण ज्ञान को खोने नहीं देता है।

तर्कसंगत स्तर
अंतिम, तार्किक चरण के बिना अनुभूति का स्तर गलत लगेगा। ऐतिहासिक रूप से, ग्रह पर अपनी उपस्थिति के क्षण से ही मनुष्य महसूस करने में सक्षम था। लेकिन मैंने सोचना, लिखना और विश्लेषण करना बहुत बाद में सीखा। यह स्तर पूर्णतः मानसिक गुणों पर निर्मित होता है। इसलिए, यह अविश्वसनीय रूप से जटिल है और उतना दृश्यात्मक नहीं है जितना कामुक है। हालाँकि, इसके लाभ बहुत अधिक हैं, खासकर जब से आधुनिक समाज के विकास के साथ यह तर्कसंगत स्तर है जिसकी मांग अधिक होती जा रही है। हमारे ग्रह पर अधिकांश वस्तुएँ पहले ही संवेदी स्तर के सभी रूपों से गुज़र चुकी हैं। इसका मतलब यह है कि उन्हें व्यवस्थित करने, रिकॉर्ड करने और कुछ निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता है।
तर्कसंगत स्तर के रूप
ये तीन प्रकार के होते हैं:
- अवधारणा। संवेदना का उपयोग करके, हमने संपत्ति का निर्धारण किया, धारणा के लिए धन्यवाद, हमने एक पूरी तस्वीर बनाई, और इस रूप का उपयोग करके, हम इसे प्रस्तुत करने में सक्षम थे। यह समझने के लिए कि नींबू का स्वाद खट्टा होता है, आपको इसे आज़माने की ज़रूरत नहीं है, बस इसके बारे में पढ़ें .
- निर्णय. यह सदैव दिशात्मक होता है। उदाहरण के लिए, वाक्यांश "नींबू खट्टा है" इस रूप का एक प्रमुख उदाहरण है। निर्णय नकारात्मक या सकारात्मक हो सकता है. लेकिन यह भी या तो एक अवधारणा पर या एक धारणा पर निर्मित होता है।
- निष्कर्ष। पिछले स्वरूप से आता है. यह उन सभी चीज़ों का सार प्रस्तुत करता है जिन्हें हमने एक उत्तर में व्यवस्थित किया है। तो, यह कहने पर कि नींबू मीठा नहीं है, जहरीला नहीं है और इसका रंग पीला है, हम इस विषय पर कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अनुमान तीन प्रकार के होते हैं: आगमनात्मक, निगमनात्मक और सादृश्यात्मक। शर्लक होम्स के बारे में कहानियाँ याद रखें। उन्होंने सामान्य निर्णयों का उपयोग करके निष्कर्ष निकालने के लिए कटौती का व्यापक उपयोग किया।
अलग से, अंतर्ज्ञान को कभी-कभी अनुभूति के एक विशेष स्तर के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है। सच है, इस घटना का अभी भी बहुत कम अध्ययन किया गया है।
उन्होंने ज्ञान का उद्देश्य प्रकृति की शक्तियों पर काबू पाने के साथ-साथ स्वयं मनुष्य को बेहतर बनाने में देखा। आधुनिक साहित्य में ज्ञान का लक्ष्य सत्य रूप में देखा जाता है।
ज्ञान के स्वरूप
वैज्ञानिक
वैज्ञानिक ज्ञान, ज्ञान के अन्य विविध रूपों के विपरीत, वस्तुनिष्ठ, सच्चा ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य वास्तविकता के नियमों को प्रतिबिंबित करना है। वैज्ञानिक ज्ञान के तीन कार्य हैं और यह वास्तविकता की प्रक्रियाओं और घटनाओं के विवरण, स्पष्टीकरण और भविष्यवाणी से जुड़ा है।
कलात्मक
संकेतों, प्रतीकों, कलात्मक छवियों के माध्यम से मौजूदा वास्तविकता का प्रतिबिंब।
दार्शनिक
दार्शनिक ज्ञान विश्व का एक विशेष प्रकार का समग्र ज्ञान है। दार्शनिक ज्ञान की विशिष्टता खंडित वास्तविकता से परे जाने और अस्तित्व के मूलभूत सिद्धांतों और नींव को खोजने, उसमें मनुष्य का स्थान निर्धारित करने की इच्छा है। दार्शनिक ज्ञान कुछ वैचारिक आधारों पर आधारित होता है। इसमें शामिल हैं: ज्ञानमीमांसा और ऑन्टोलॉजी। दार्शनिक अनुभूति की प्रक्रिया में, विषय न केवल मनुष्य के अस्तित्व और स्थान को समझने का प्रयास करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि उन्हें क्या होना चाहिए (स्वयंसिद्धांत), यानी, वह एक आदर्श बनाने का प्रयास करता है, जिसकी सामग्री होगी दार्शनिक द्वारा चुने गए विश्वदृष्टि अभिधारणाओं द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए।
पौराणिक
पौराणिक ज्ञान आदिम संस्कृति की विशेषता है। ऐसा ज्ञान अलौकिक प्राणियों, महान नायकों की संवेदी-दृश्य छवियों की मदद से वास्तविकता की समग्र पूर्व-सैद्धांतिक व्याख्या के रूप में कार्य करता है, जो पौराणिक ज्ञान के वाहक के लिए उसके रोजमर्रा के जीवन में वास्तविक भागीदार प्रतीत होते हैं। पौराणिक ज्ञान की विशेषता मानवीकरण, देवताओं और मानवरूपता की छवियों में जटिल अवधारणाओं का मानवीकरण है।
धार्मिक
एकेश्वरवादी धर्मों, अर्थात् यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम में धार्मिक ज्ञान का उद्देश्य ईश्वर है, जो स्वयं को एक विषय, एक व्यक्ति के रूप में प्रकट करता है। धार्मिक ज्ञान का कार्य, या विश्वास का कार्य, एक व्यक्तिगत-संवादात्मक चरित्र है। एकेश्वरवाद में धार्मिक ज्ञान का लक्ष्य ईश्वर के बारे में विचारों की एक प्रणाली का निर्माण या स्पष्टीकरण नहीं है, बल्कि मनुष्य का उद्धार है, जिसके लिए एक ही समय में ईश्वर के अस्तित्व की खोज आत्म-खोज का कार्य बन जाती है। , आत्म-ज्ञान और उसकी चेतना में नैतिक नवीनीकरण की मांग का निर्माण करता है।
वैज्ञानिक ज्ञान का स्तर
वैज्ञानिक ज्ञान के दो स्तर हैं: अनुभवजन्य (अनुभवी, संवेदी) और सैद्धांतिक (तर्कसंगत)। ज्ञान का अनुभवजन्य स्तर अवलोकन और प्रयोग में व्यक्त किया जाता है, जबकि सैद्धांतिक स्तर परिकल्पनाओं, कानूनों और सिद्धांतों में अनुभवजन्य स्तर के परिणामों के सामान्यीकरण में होता है।
अवधारणा का इतिहास
प्लेटो
यह सभी देखें
टिप्पणियाँ
साहित्य
- कोखानोव्स्की वी.पी. एट अल। विज्ञान के दर्शन के मूल सिद्धांत। एम.: फीनिक्स, 2007. आईएसबीएन 978-5-222-11009-6 के साथ 608
- ज्ञान के सिद्धांत के लिए, ब्रॉकहॉस और एफ्रॉन शब्दकोश या ग्रेट सोवियत इनसाइक्लोपीडिया देखें।
लिंक
- फ्रोलोव आई. टी. "दर्शनशास्त्र का परिचय" / अध्याय VI। "अनुभूति"
विकिमीडिया फ़ाउंडेशन. 2010.
समानार्थी शब्द:देखें अन्य शब्दकोशों में "अनुभूति" क्या है:
एक श्रेणी जो गतिविधि और संचार के लिए आदर्श योजनाओं को दोहराकर, संकेत-प्रतीकात्मक प्रणाली बनाकर किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने की प्रक्रिया का वर्णन करती है जो किसी व्यक्ति की दुनिया और अन्य लोगों के साथ बातचीत में मध्यस्थता करती है। दर्शन पी. की अवधारणाएँ अत्यंत... ... दार्शनिक विश्वकोश
समझ देखें... रूसी पर्यायवाची और समान अभिव्यक्तियों का शब्दकोश। अंतर्गत। ईडी। एन. अब्रामोवा, एम.: रूसी शब्दकोश, 1999. ज्ञान ज्ञान, समझ; समझ, अध्ययन; निपुणता, निपुणता, आत्मसात रूसी शब्दकोश ... पर्यायवाची शब्दकोष
अनुभूति- अनुभूति एक दार्शनिक श्रेणी है जो गतिविधि और संचार के लिए आदर्श योजनाओं के निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन करती है, संकेत-प्रतीकात्मक प्रणाली बनाती है जो विभिन्न के संश्लेषण में दुनिया और अन्य लोगों के साथ एक व्यक्ति की बातचीत में मध्यस्थता करती है... ... ज्ञानमीमांसा और विज्ञान के दर्शन का विश्वकोश
अनुभूति- अनुभूति ♦ Connaissance जानने का अर्थ है जो है, जैसा है वैसा ही समझना। अनुभूति विषय और वस्तु के बीच, आत्मा और दुनिया के बीच, या संक्षेप में, वेरिटास इंटेलेक्चस (सत्य...) के बीच एक प्रकार का पर्याप्त संबंध है। स्पोनविले का दार्शनिक शब्दकोश
अनुभूति, ज्ञान, सीएफ। (किताब)। 1. केवल इकाइयाँ चौ. के तहत कार्रवाई 1 मान में जानिए जानने के; जानने की क्षमता; किसी व्यक्ति द्वारा अपने आप में किसी चीज़ के सरल और स्पष्ट परिवर्तन को घटना में, उसके लिए एक चीज़ (दर्शन) में बदलना। "द्वंद्वात्मक... ... उशाकोव का व्याख्यात्मक शब्दकोश
अनुभूति- अनुभूति, समझ, समझ, पहचान, पकड़, किताबों की समझ। संज्ञानात्मकता, बोधगम्यता, पुस्तकों की पहचान। जानने योग्य, समझने योग्य, पहचानने योग्य जानने/जानने योग्य, समझने योग्य/समझने योग्य और समझने योग्य, समझने योग्य/समझने योग्य... रूसी भाषण के पर्यायवाची का शब्दकोश-थिसॉरस
अनुभूति- किसी चीज़ की समझ, किसी चीज़ के बारे में ज्ञान प्राप्त करना; कुछ घटनाओं, प्रक्रियाओं आदि के नियमों की समझ। एक व्यावहारिक मनोवैज्ञानिक का शब्दकोश। एम.: एएसटी, हार्वेस्ट। एस यू गोलोविन। 1998. अनुभूति... महान मनोवैज्ञानिक विश्वकोश
विषय की सोच में वास्तविकता को प्रतिबिंबित करने और पुन: प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, जिसका परिणाम दुनिया के बारे में नया ज्ञान है... बड़ा विश्वकोश शब्दकोश
विषय की रचनात्मक गतिविधि, दुनिया के बारे में विश्वसनीय ज्ञान प्राप्त करने पर केंद्रित है। पी. संस्कृति के अस्तित्व की एक अनिवार्य विशेषता है और, इसके कार्यात्मक उद्देश्य के आधार पर, ज्ञान की प्रकृति और संबंधित साधन और ... नवीनतम दार्शनिक शब्दकोश